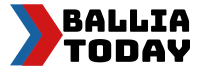News Desk : अफगानिस्तान की सत्ता में तालिबान की वापसी को लेकर कुछ भारतीय मीडिया प्लेटफार्म्स और कथित सामरिक विशेषज्ञ बेवजह भ्रम फैला रहे हैं। उन्हें यह तालिबान के समक्ष अमेरिका के समर्पण जैसा कुछ लग रहा है। कुछ को इसमें वियतनाम की छवि दिखाई दे रही है, मानो वियतनामियों की तरह तालिबान ने लड़ते हुए अमेरिकी सैनिकों को अपने मुल्क से भगा दिया हो। तालिबान को अफगानिस्तान की सत्ता अमेरिकी सेना से लड़कर नहीं, दोनों शक्तियों (तालिबान और अमेरिकी सरकार) की किसी अघोषित दुरभिसंधि के तहत मिली है। इसके लिए तालिबान को कोई खास संघर्ष नहीं करना पड़ा। बारी-बारी से वे अफगानिस्तानी प्रदेशों को जीतते रहे और फिर काबुल आ पहुंचे। अमेरिका और नाटो द्वारा प्रशिक्षित और संपोषित अफगानिस्तान की तकरीबन 3 लाख 50 हजार की सेना और पुलिस ने 50-60 हजार की संख्या वाले तालिबान सशस्त्र उग्रवादियों का कहीं भी खास प्रतिरोध नहीं किया। सिर्फ हेरात और लश्करगाह जैसे कुछ इलाकों में ही थोड़ा-बहुत प्रतिरोध हुआ। अमेरिकी-छत्रछाय़ा में चलने वाली अफगानिस्तान की पिट्ठू अशरफ गनी सरकार ने तालिबान के काबुल में घुसने से पहले ही समर्पण कर दिया और सिर्फ राष्ट्रपति भवन ही नहीं, अपना मुल्क छोड़कर भाग गये। ऐसा लगता है, मानो अशरफ गनी को सब कुछ मालूम था कि उन्हें कब-क्या करना है। अफगानिस्तान की पूर्व सरकार में चीफ एक्जीक्यूटिव रहे अब्दुल्ला अब्दुल्ला और गनी सरकार में रक्षा मंत्री रहे जनरल बिस्मिल्लाह मोहम्मदी भी अब यह बात खुल कर कह रहे हैं। इन तथ्यों से सबसे पहली बात उभरती है कि तालिबान की कथित विजय और सत्ता में वापसी की तुलना वियतनामी जनता के अमेरिका-विरोधी गौरवशाली संघर्ष और महान् विजय से नहीं की जानी चाहिए। ऐसा करके भारत के कुछ अंग्रेजी-हिन्दी चैनल वियतनाम और उसकी जनता का अपमान कर रहे हैं। पता नहीं, वे यह सब अज्ञानतावश कर रहे हैं या किसी योजना के तहत? दूसरी बात कि तालिबान को सत्ता में वापसी का यह रास्ता बनाने की प्रक्रिया पिछले एक साल से चल रही थी। इसके लिए दोहा और वाशिंगटन में लगातार बैठकें, खुले और गोपनीय विमर्श होते रहे। यह बात सही है कि इस प्रक्रिया में अमेरिका ने कुछ अन्य मुल्कों को भी शरीक किया, खासतौर पर ऐसे कुछ मुल्कों को जिनकी सरहदें अफगानिस्तान से मिलती हैं। सरहदी देश न होने के चलते भारत को इसमें सीधे तौर पर कभी शामिल नहीं किया गया। हालांकि अमेरिकी शासन अफगानिस्तान में भारत के बड़े निवेश और अन्य हितों से अच्छी तरह वाकिफ था। इस पूरी प्रक्रिया में आज भारत की कूटनीतिक दयनीयता भी उजागर हुई है। किसी खास अमेरिकी-फार्मूले के तहत ही काबुल में तालिबान की इतने सहज ढंग से वापसी हुई है। अशरफ़ गनी भी किसी खास अमेरिकी फार्मूले के तहत ही अफगानिस्तान के राष्ट्रपति बने थे। अफगानिस्तान की जनता या राजनीति में उनकी कभी कोई हैसियत नहीं थी। मजे की बात कि अभी दो दिन पहले तक जिन अली अहमद जलाली को संक्रमण कालीन सरकार का प्रमुख या अशरफ़ गनी का उत्तराधिकारी बनाने की बात चल रही थी, वह भी अमेरिका की ही पसंद थे। वह तो वर्षों से अमेरिकी नागरिक हैं। पद से हट चुके अशरफ़ गनी भी सन् 1964 से 2009 के बीच अमेरिकी नागरिक थे। समझा जाता है कि अफगानी मूल के अमेरिकी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अहमद जलाली को कुछ समय तक शासन का प्रमुख बनाने की तालिबान ने पहले अपनी मंजूरी दे दी थी। पर अब सत्ता का संचालन किसी संक्रमणकालीन सरकार के बगैर उसने स्वयं ही करने का फैसला किया है। तालिबान ने साफ कर दिया है कि अब कोई अंतरिम या संक्रमणकालीन सरकार नहीं होगी। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि तकरीबन दो दशक से अफगानिस्तान में जो भी होता आ रहा है, वह दुनिया भर में सत्ता-पलट के कुख्यात षड्यंत्रकारी-अमेरिका के नक्शेकदम पर ही। अभी जो हो रहा है, वह भी अमेरिका के ही नक्शेकदम पर है। इसमें किसी को भ्रम नहीं होना चाहिये। अमेरिका को अफगानिस्तान से हटना था। वह उसकी अपनी मजबूरी रही होगी। लेकिन अपनी मजबूरी को उसने निश्चय ही किसी ठोस योजना और रणनीति से जोड़ा होगा। यह महज संयोग नहीं कि अमेरिका हो या ब्रिटेन जैसा उसका कोई भी सहयोगी देश एक बार भी तालिबान की सत्ता-वापसी पर अफसोस य़ा दुखद आश्चर्य नहीं प्रकट किया है। कल ब्रिटिश सरकार के प्रवक्ता और स्वयं प्रधानमंत्री जानसन ने भी माना कि अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता अब एक सच्चाई है। इससे तो यही लगता है कि ये देश जल्दी ही उसे अपनी कूटनीतिक मंजूरी भी दे देंगे। देखना है कि भारत इस मामले में कब तक असमंजस में झूलेगा। दोहा में वार्ताओं के लंबे दौर से बिल्कुल साफ था कि अमेरिका अपने कुछ मित्र-देशों से मशविरे के बाद अफगानिस्तान में सत्ता-हस्तांतरण के लिए नया प्रकल्प तैयार किया। क्या यह प्रकल्प उसके लिए फायदेमंद नहीं होगा। क्या इसका फायदा चीन-रूस या पाकिस्तान उठा सकते हैं। अटकलों की शक्ल में ऐसे भी कुछ सवाल उठाये जा रहे हैं। एक भारतीय पत्रकार के तौर पर भारत-पाकिस्तान मामलों, खासकर कश्मीर मसले को समझने की लगातार कोशिश करता रहा हूं। इसमें अफगानिस्तान का पहलू कई बार अचानक उभर आता रहा है। ऐसे में अमेरिका के इस नये ‘अफगानिस्तान-प्रकल्प’ को भारत ही नहीं, रूस और चीन के लिए भी बहुत आश्वस्तकारी नहीं माना जा सकता। यह बहुत कुछ तालिबान पर निर्भर करेगा कि वह अमेरिका की कब तक हां मे हां मिलाता रहेगा और कब किसी और धुरी की तरफ जा झुकेगा। जहां तक अमेरिका का सवाल है, उसे तालिबान क्या, दुनिया के किसी भी पिछड़े या अविकसित या विकासशील देश में किसी भी निरंकुश सरकार से कभी परहेज नहीं रहा बशर्ते कि वह अमेरिकी हितों को महत्व देती रहे। तालिबान सरकार के साथ भी उसका यही रुख रहेगा। अफगानिस्तान में भी अगर यही समीकरण जारी रहा तो भविष्य में उसके कुछ खतरनाक आयाम उभर सकते हैं। इसीलिए, भारत, रूस और चीन तीनों मुल्कों की सरकारों और सामरिक मामलों के उनके विशेषज्ञों को इस ‘अनोखे सत्ता-हस्तांतरण’ के अमेरिकी राजनीतिक-प्रकल्प को लेकर आश्वस्त होने से ज्यादा सतर्क रहना चाहिए।
(उर्मिलेश वरिष्ठ पत्रकार होने के साथ कई किताबों के लेखक हैं।)